भारत में शादी केवल धार्मिक या सामाजिक रस्मों का हिस्सा नहीं रह गई है, बल्कि अब यह एक कानूनी अनुबंध भी है। जब युवा जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति या पारिवारिक दबावों से परे जाकर जीवनसाथी चुनना चाहते हैं, तब कोर्ट मैरिज एक व्यावहारिक और सुरक्षित विकल्प बन जाता है। यह विवाह प्रणाली स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कानून की निगरानी में पूरी होती है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए आदर्श है जो बिना दहेज, सामाजिक तामझाम या पारिवारिक दबाव के विवाह करना चाहते हैं।
प्रेरणादायक कानूनी विचार: “विवाह एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, और व्यक्ति को अपने जीवनसाथी का चयन करने का अधिकार है।”— सुप्रीम कोर्ट, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006
कोर्ट मैरिज क्या होती है?
भारत में विवाह के लिए अलग-अलग धार्मिक कानून मौजूद हैं, जैसे कि:
- Hindu Marriage Act, 1955 – यह कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य होते हैं, जैसे सप्तपदी और पाणिग्रहण।
- Muslim Personal Law (Shariat) – इस्लामी विवाह को एक निकााह (सिविल कॉन्ट्रैक्ट) माना जाता है, जो मेहर, कुबूल और गवाहों की उपस्थिति में होता है। इसमें कुरान और हदीस की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है।
हालांकि, जब दो व्यक्ति अलग-अलग धर्मों से होते हैं, या जब कोई जोड़ा पारंपरिक धार्मिक विधानों से विवाह नहीं करना चाहता, तब Special Marriage Act, 1954 के तहत कोर्ट मैरिज एक कानूनी विकल्प बन जाता है। इस कानून में:
- विवाह पूरी तरह धर्म-निरपेक्ष होता है।
- किसी भी धार्मिक रिवाज की आवश्यकता नहीं होती।
- विवाह केवल आपसी सहमति, गवाहों और रजिस्ट्रार की निगरानी में होता है।
- अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह की पूरी स्वतंत्रता होती है।
इसलिए, जब दंपती चाहते हैं कि उनका विवाह धर्म और परंपरा से स्वतंत्र हो, या उन्हें सामाजिक दबावों से बचना है, तो वे Special Marriage Act का चयन करते हैं। यह खासकर लव मैरिज, अंतरजातीय विवाह या अंतर-धार्मिक विवाह के मामलों में सबसे उपयुक्त होता है।
कोर्ट मैरिज, भारत के विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत होती है, जो अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह की अनुमति देता है। इसमें दो बालिग व्यक्ति, आपसी सहमति से विवाह कर सकते हैं, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति से हों। इस प्रक्रिया में किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती और अंत में विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र विवाह के कानूनी सबूत के रूप में मान्य होता है, जिसे सरकारी दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सकता है।
कोर्ट मैरिज और पारंपरिक विवाह में अंतर
कोर्ट मैरिज और पारंपरिक विवाह के बीच मुख्य अंतर उनकी प्रकृति, प्रक्रिया और उद्देश्य में होता है। कोर्ट मैरिज पूरी तरह कानूनी और दस्तावेज़ आधारित प्रक्रिया होती है, जबकि पारंपरिक विवाह सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है।
कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के दो बालिग व्यक्तियों के बीच सहमति से हो सकता है, वहीं पारंपरिक विवाह में अक्सर सामाजिक परंपराओं और परिवार की सहमति को महत्व दिया जाता है। कोर्ट मैरिज में पारदर्शिता और कम खर्च होता है, जबकि पारंपरिक विवाह भव्यता और सामाजिक रस्मों पर आधारित होता है। कोर्ट मैरिज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा मिलती है।
| तत्व | कोर्ट मैरिज | पारंपरिक विवाह |
| प्रक्रिया | कानूनी, रजिस्ट्रार के समक्ष | धार्मिक, रीति-रिवाजों के अनुसार |
| गवाह | आवश्यक (कम से कम 2) | कभी-कभी अनौपचारिक |
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | कई बार मौखिक सहमति पर्याप्त |
| खर्च | कम | अधिक, समारोह आदि के कारण |
| समय | सीमित, निर्धारित | कई बार लंबा |
पात्रता (Eligibility Criteria)
कोर्ट मैरिज के लिए वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और विवाह की समझ व सहमति होनी चाहिए। यदि पहले से शादीशुदा थे, तो तलाक या विधवा होने का प्रमाण आवश्यक है। दोनों पक्षों का विवाह के लिए स्वतंत्र होना अनिवार्य है।
कानूनी उद्धरण:
विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह एक सिविल अनुबंध है। इसमें किसी धार्मिक समारोह की आवश्यकता नहीं होती।— जस्टिस एस. एस. निज्जर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया
जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज़ आवश्यक है।
- आयु प्रमाण: 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- पासपोर्ट साइज फोटो: दोनों पक्षों की 6-6 तस्वीरें जरूरी हैं।
- पूर्व विवाह का प्रमाण: तलाक प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- गवाहों के दस्तावेज़: दो गवाहों के आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य हैं।
- निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, राशन कार्ड या पासपोर्ट आदि चलेंगे।
स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझते है
1) नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज (Notice of Intended Marriage)
शादी से पहले दोनों पक्ष रजिस्ट्रार कार्यालय में फॉर्म भरकर अपने विवाह का इरादा घोषित करते हैं। यह फॉर्म उसी जिले में जमा करना होता है, जहां दोनों में से कोई एक कम से कम 30 दिनों से निवास कर रहा हो। साथ ही दोनों को अपनी पहचान और निवास का प्रमाण देना होता है।
2) 30 दिन की सार्वजनिक नोटिस अवधि
नोटिस जमा करने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में इसे 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यदि इस दौरान किसी को विवाह से कोई आपत्ति हो, तो वह लिखित रूप में उसे दर्ज करा सकता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए होती है।
3) आपत्ति न आने की स्थिति में विवाह की तारीख तय होना
अगर 30 दिनों तक कोई आपत्ति नहीं आती है, तो विवाह की तारीख रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस दिन वर और वधू को दो गवाहों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होता है। विवाह की प्रक्रिया उसी दिन पूरी की जाती है।
4) दस्तावेजों का सत्यापन और शपथ ग्रहण
विवाह के दिन दोनों पक्षों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद वर और वधू एक-दूसरे के प्रति विवाह की सहमति व्यक्त करते हैं और कानून के अनुसार शपथ लेते हैं। यह शपथ विवाह अधिकारी के समक्ष ली जाती है।
5) विवाह प्रमाण पत्र जारी होना
सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र भविष्य में कानूनी आवश्यकताओं, वीज़ा, पासपोर्ट, नाम परिवर्तन आदि में सहायक होता है। यह प्रमाण पत्र विवाह का एकमात्र वैध कानूनी प्रमाण है।
संबंधित न्यायिक निर्णय
- शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. (2018): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, चाहे वह अंतर-धार्मिक हो। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
- लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006): सुप्रीम कोर्ट ने अंतर-जातीय विवाह को वैध और प्रोत्साहन योग्य बताया। अदालत ने कहा कि ऐसे विवाहों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट मैरिज के लाभ
- धर्म और जाति की बाध्यता नहीं: कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता है।
- कानूनी सुरक्षा: विवाह प्रमाण पत्र वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
- कम खर्चीला: पारंपरिक विवाह की तुलना में यह काफी सस्ता होता है।
- वीज़ा और पासपोर्ट: कानूनी विवाह होने के कारण दस्तावेज़ों में आसानी होती है।
- सहूलियत: पूरी प्रक्रिया सीमित समय और पारदर्शिता के साथ होती है।
मानव-केंद्रित सुझाव
- माता-पिता को जानकारी देना: यदि संभव हो तो परिवार को विवाह के बारे में अवश्य बताएं।
- दस्तावेज़ समय से तैयार करें: सभी जरूरी दस्तावेज पहले से इकट्ठा कर लें ताकि कोई देरी न हो।
- कानूनी सलाह लें: अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय विवाह में वकील की सलाह लें।
- ऑनलाइन आवेदन सावधानी से करें: जानकारी सही भरें ताकि आवेदन निरस्त न हो।
- साक्षात्कार की तैयारी करें: विवाह अधिकारी आपके इरादे की जांच कर सकते हैं।
कहां आवेदन करें?
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए संबंधित पोर्टल को जरूर जांचें।
कुछ प्रमुख राज्य पोर्टल्स:
- दिल्ली: https://edistrict.delhigovt.nic.in
- महाराष्ट्र: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
- उत्तर प्रदेश: https://igrsup.gov.in
निष्कर्ष
कोर्ट मैरिज न केवल एक कानूनी विवाह का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। यह स्वतंत्रता, समानता और निजता को सम्मान देने वाला माध्यम है। यदि आप भी कोर्ट मैरिज की योजना बना रहे हैं, तो आज ही Marriage Registrar से संपर्क करें या अनुभवी वकीलों से मार्गदर्शन लें।
किसी भी कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की पूरी टीम है, जो आपकी हर संभव सहायता करेगी।
FAQs
1. क्या कोर्ट मैरिज में परिवार की अनुमति जरूरी है?
उत्तर: नहीं, केवल वर और वधू की आपसी सहमति ही पर्याप्त है।
2. क्या दोनों का एक ही धर्म होना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट सभी धर्मों के व्यक्तियों को विवाह की अनुमति देता है।
3. कितने गवाहों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: कम से कम दो गवाहों की जरूरत होती है जिनके पास वैध पहचान प्रमाण होना चाहिए।
4. क्या कोर्ट मैरिज ऑनलाइन हो सकती है?
उत्तर: कुछ राज्यों में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन विवाह का अंतिम चरण रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होता है।
5. क्या कोर्ट मैरिज तुरंत हो जाती है?
उत्तर: नहीं, प्रक्रिया में न्यूनतम 30 दिन का समय लगता है क्योंकि नोटिस की अवधि अनिवार्य होती है।

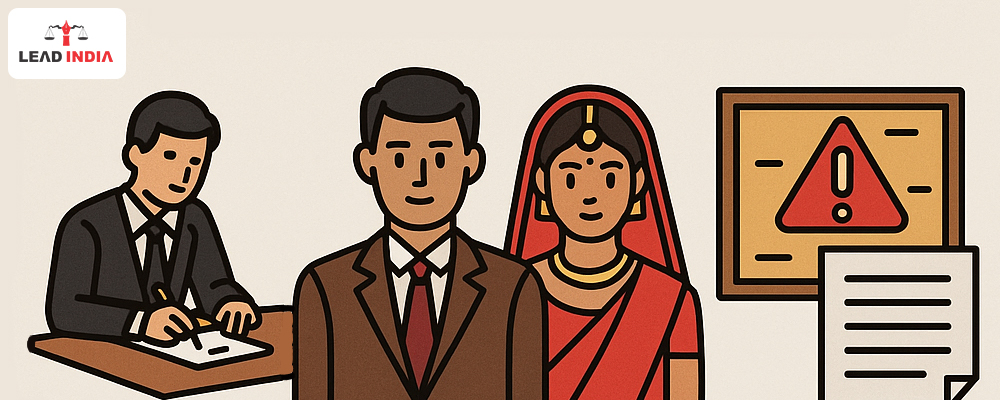




 एडवोकेट से पूछे सवाल
एडवोकेट से पूछे सवाल